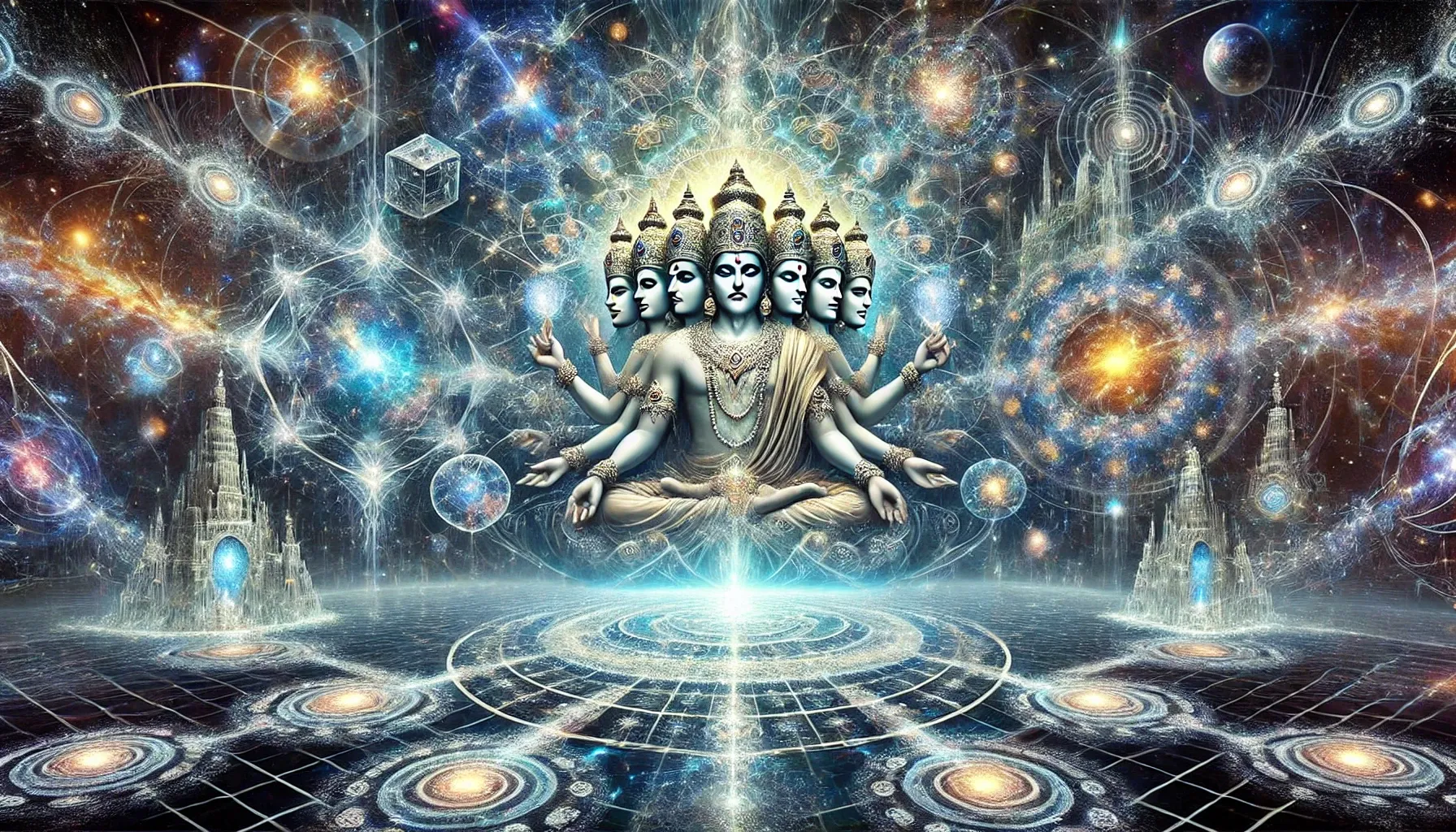भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय(हिन्दी अनुवाद)।यहाँ पर भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय(हिन्दी अनुवाद) के सभी श्लोकों के साथ हिन्दी अनुवाद क्रमशः है
भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय(हिन्दी अनुवाद)
यहाँ पर भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय(हिन्दी अनुवाद) के सभी श्लोकों के साथ हिन्दी अनुवाद क्रमशः प्रस्तुत किया गया है।
॥ श्रीशुक उवाच ॥
श्लोक 1:
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः।
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥
अनुवाद:
यहां सर्ग (सृष्टि) और विसर्ग (विसर्जन), स्थान (विराट रूप), पोषण और ऊतय (पुनर्निर्माण) के बारे में वर्णन किया गया है। मन्वंतर के विषय में चर्चा की जाएगी, जिसमें निरोध (अवस्था) और मुक्ति की बात होगी, जो सभी के लिए आश्रय का कारण है।
श्लोक 2:
दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्।
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥
अनुवाद:
इस श्लोक में दशम (विष्णु के दस अवतारों) के विशुद्ध रूप से समझने के लिए, महात्मा भक्तों द्वारा उनके लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। ये लक्षण शास्त्रों और सही अर्थ के अनुसार बताए गए हैं।
श्लोक 3:
भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः।
ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः ॥
अनुवाद:
सभी भूतों की इंद्रिय भावना के अनुसार जन्म और सर्ग का प्रसंग उपदेशित किया गया है। ब्रह्मा के गुणों के वैषम्य के कारण विसर्ग (सृष्टि) और पौरुष (पुरुषत्व) का स्मरण किया गया है।
श्लोक 4:
स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः।
मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः ॥
अनुवाद:
भगवान के धाम (वैकुण्ठ) की स्थिति, उनके विजय की क्रिया, पोषण और अनुग्रह की प्रक्रियाएं, मन्वंतर के दौरान सद्धर्म की प्रतिष्ठा और कर्मों के वासनाओं का आयोजन इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है।
श्लोक 5:
अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम्।
पुंसां ईशकथाः प्रोक्ता नानाख्यान उपबृंहिताः ॥
अनुवाद:
भगवान के अवतारों की कथा और उनके साथ जुड़ी उपाख्यानों का प्रचार किया गया है। यह श्लोक उन कथाओं को संदर्भित करता है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों द्वारा दी गईं।
श्लोक 6:
निरोधोऽस्यानुशयनं आत्मनः सह शक्तिभिः।
मुक्तिः हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥
अनुवाद:
निरोध (विलीनता) और मुक्ति की स्थिति में आत्मा अपनी शक्तियों के साथ अपने असली रूप में स्थित होती है, और वह रूप स्वाभाविक रूप से वास करता है।
श्लोक 7:
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते।
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥
अनुवाद:
आभास (दृश्य रूप) और निरोध (विलीनता) की प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है जब परब्रह्म के आश्रय में ध्यान किया जाता है। इस प्रक्रिया को परमात्मा के शब्दों द्वारा संज्ञापित किया जाता है।
श्लोक 8:
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसौ एवाधिदैविकः।
यः तत्र उभय विच्छेदः स स्मृतोह्याधिभौतिकः ॥
अनुवाद:
यह पुरुष आत्मिक रूप से दिव्य है और जब वह अपने शरीर में विचलित होता है, तब वह भौतिक रूप से पहचान में आता है। यह दोनों ही रूपों में सक्रिय रहता है।
श्लोक 9:
एकं एकतराभावे यदा न उपलभामहे।
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥
अनुवाद:
जब कोई एकता और भिन्नता के बीच भेद नहीं देख पाता, तब वही व्यक्ति त्रैतीय (तीनों रूपों) को समझ सकता है और उसकी आत्मा के सही आश्रय का अनुभव करता है।
श्लोक 10:
पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदाऽसौ स विनिर्गतः।
आत्मनोऽयनमन्विच्छन् अपः अस्राक्षीच्छुचिः शुचीः ॥
अनुवाद:
जब पुरुष अंड (ब्रह्मांड) को छोड़ता है, तब वह आत्म के सही मार्ग का अनुसरण करता है और शुद्धता को प्राप्त करता है।
श्लोक 11:
तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्।
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः ॥
अनुवाद:
भगवान नारायण ने अपने दिव्य नाम से उन जीवों को सृष्टि के द्वारा पुनः जन्म दिया, और फिर वे जीवन के चक्र से बाहर निकलते हुए पुनः आकाश में लौट आए।
श्लोक 12:
द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च।
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद् उपेक्षया ॥
अनुवाद:
सभी द्रव्य (संसार), कर्म, काल, और स्वभाव के द्वारा जीवों का निर्माण होता है। जो भगवान के आशीर्वाद से होते हैं, वही सचमुच अस्तित्व में आते हैं।
श्लोक 13:
एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः।
वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा ॥
अनुवाद:
भगवान ने अपनी शक्ति और माया से तीन रूपों में यह सृष्टि उत्पन्न की। जब वह स्वयं अपनी एकता को मानते हुए विभिन्न रूपों में फैलते हैं, तब वह शक्तियों के द्वारा संसार का निर्माण करते हैं।
श्लोक 14:
अधिदैवं अथ अध्यात्मं अधिभूतमिति प्रभुः।
अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु॥
अनुवाद:
भगवान ने कहा: "सृष्टि के तीन प्रमुख पहलु हैं: अधिदैविक, अध्यात्मिक और अधिभौतिक। इन तीनों के द्वारा भगवान की शक्ति का त्रिविध विभाजन होता है।"
श्लोक 15:
अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः।
ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महान् असुः॥
अनुवाद:
मनुष्य के शरीर में आकाश से जुड़ी हुई शक्ति, ओज, बल, और अन्य जीवात्माओं की जैसी दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इससे उत्पन्न प्राण शक्ति महान होती है।
श्लोक 16:
अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु।
अपानंतं अपानन्ति नरदेवं इवानुगाः॥
अनुवाद:
प्राणियों के भीतर प्राण शक्ति व्याप्त होती है, और प्राणों के द्वारा सभी जीवों को जीवन मिलता है। अपान (नीचे की दिशा में) भी उस प्राण शक्ति के द्वारा कार्य करता है।
श्लोक 17:
प्राणेन आक्षिपता क्षुत् तृड् अन्तरा जायते विभोः।
पिपासतो जक्षतश्च प्राङ् मुखं निरभिद्यत॥
अनुवाद:
प्राण की क्रिया से शरीर में भूख और प्यास उत्पन्न होती है, और यह प्रक्रिया प्रभु के अस्तित्व से ही संभव होती है। इससे सभी जीवों में जिव्हा के द्वारा विभिन्न स्वादों का अनुभव होता है।
श्लोक 18:
मुखतः तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्र उपजायते।
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते॥
अनुवाद:
मुख के तालू से जुड़ी जिह्वा से विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं, और यह सारे स्वाद मनुष्य द्वारा अनुभव किए जाते हैं।
श्लोक 19:
विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग् व्याहृतं तयोः।
जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत॥
अनुवाद:
मुख से निकलने वाली वाणी, जल और अग्नि का समन्वय करती है। इस प्रक्रिया से शरीर में ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है, और यह सब भगवान के परम तत्व से नियंत्रित होता है।
श्लोक 20:
नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति।
तत्र वायुः गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः॥
अनुवाद:
नाक से गंध का अनुभव होता है, जो वायु के माध्यम से फैलता है। यह गंध जीवन में विभिन्न अहसासों का स्रोत बनती है।
श्लोक 21:
यदाऽऽत्मनि निरालोकं आत्मानं च दिदृक्षतः।
निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिः चक्षुः गुणग्रहः॥
अनुवाद:
जब व्यक्ति अपने आत्मा को देखता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसकी आंखों की ज्योति और गुणों की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है।
श्लोक 22:
बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनः तत् जिघृक्षतः।
कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः॥
अनुवाद:
जो व्यक्ति आत्मज्ञान में ध्यान केंद्रित करता है, उसके कानों में गुणों का समावेश होता है और उसका श्रोत्र शक्तिशाली होता है। वह दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होता है।
श्लोक 23:
वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुर्वोष्ण शीतताम्।
जिघृक्षतः त्वङ् निर्भिन्ना तस्यां रोम महीरुहाः।
अनुवाद:
जिसे वस्तु की संवेदनाओं के द्वारा सुगमता और कठोरता का अहसास होता है, उसका तन और रोम-रंध्र सक्रिय हो जाते हैं, और वह बाहरी और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव करता है।
श्लोक 24:
हस्तौ रुरुहतुः तस्य नाना कर्म चिकीर्षया।
तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानं उभयाश्रयम्॥
अनुवाद:
जब व्यक्ति अपने हाथों से विभिन्न कार्य करता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, और यह कार्य शक्ति और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ होता है।
श्लोक 25:
गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्।
पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः॥
अनुवाद:
जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वह निःस्वार्थ रूप से कर्म करता है, और वह अपने कार्यों के माध्यम से यज्ञ और श्रद्धा का पालन करता है।
श्लोक 26:
निरभिद्यत शिश्नो वै प्रजानन्द अमृतार्थिनः।
उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तद् उभयाश्रयम्॥
अनुवाद:
जब शिश्न (जननेंद्रिय) को विख्यात किया जाता है, तब वह प्रजनन और आनंद की प्राप्ति का स्रोत बनता है। यही वह माध्यम है जिससे कामनाओं की पूर्ति होती है।
श्लोक 27:
उत्सिसृक्षोः धातुमलं निरभिद्यत वै गुदम्।
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः॥
अनुवाद:
जब शरीर के सभी अंगों को क्रियाशील किया जाता है, तब इन अंगों के संचालन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा विभिन्न शक्तियों और स्रोतों के साथ जुड़ी होती है।
श्लोक 28:
आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारं अपानतः।
तत्र अपानः ततो मृत्युः पृथक्त्वं उभयाश्रयम्॥
अनुवाद:
जो व्यक्ति अपने पाचन और उत्सर्जन के प्रवाह को समझता है, वह उस ज्ञान का पालन करते हुए मृत्यु और जीवन के भेद को समझता है।
श्लोक 29:
आदित्सोः अन्नपानानां आसन् कुक्ष्यन्न नाडयः।
नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तदाश्रये॥
अनुवाद:
आदित्स (प्रकाश) और आन्न (भोजन) के माध्यम से शरीर के अन्न पथ और नाड़ियों में ताजगी और शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है।
श्लोक 30:
निदिध्यासोः आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत।
ततो मनः ततश्चंद्रः सङ्कल्पः काम एव च॥
अनुवाद:
जब मन आत्मा की माया में स्थित होता है, तो हृदय में शांति और मन में स्वच्छता का अहसास होता है, जिससे कामनाओं और संकल्पों की दिशा निर्धारित होती है।
श्लोक 31:
त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः।
भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायुभिः॥
अनुवाद:
शरीर में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, अस्थि, और विभिन्न तत्वों से सात प्रकार की प्राण शक्ति निवास करती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों से जुड़ी होती है।
श्लोक 32:
गुणात्मकान् इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः।
मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी॥
अनुवाद:
इंद्रियों और गुणों के माध्यम से सभी भूतों का अभ्युदय होता है। मन विकारात्मक होता है और बुद्धि और ज्ञान के रूप में कार्य करती है।
श्लोक 33:
एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया।
मह्यादिभिश्च आवरणैः अष्टभिः बहिरावृतम्॥
अनुवाद:
यह भगवद रूप स्थूल रूप में मैंने देखा है, जो आठ आवरणों द्वारा बाहरी रूप से ढका हुआ है।
श्लोक 34:
अतः परं सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणम्।
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ् मनसः परम्॥
अनुवाद:
उससे परे सूक्ष्मतम, अव्यक्त और निरविशेष रूप है, जो अनादि और अनंत काल से व्याप्त है, और जो वाणी और मन से परे है।
श्लोक 35:
अमुनी भगवद् रूपे मया ते ह्यनुवर्णिते।
उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः॥
अनुवाद:
मैंने भगवान के रूप का जो वर्णन किया है, उसे वे लोग नहीं समझ सकते जो माया से भ्रमित हैं। वे केवल बाहरी रूप को देख पाते हैं, लेकिन उनका आंतरिक अनुभव मायामय होता है।
श्लोक 36:
स वाच्य वाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक्।
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः॥
अनुवाद:
भगवान ब्रह्म के रूप में नाम, रूप और क्रिया के माध्यम से इस सृष्टि को चलाते हैं। वह कर्म और अकर्म दोनों रूपों में कार्य करने में सक्षम होते हैं।
श्लोक 37:
प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक्।
सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुर गुह्यकान्॥
अनुवाद:
भगवान ने प्रजापतियों, मुनियों, देवताओं, ऋषियों और पितरों समेत सभी जीवों के विभिन्न वर्गों का निर्माण किया। इन सभी का पालन करने वाले सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, और असुर तथा गूढ़ ज्ञान के स्वामी हैं।
श्लोक 38:
किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किम्पुरुषोरगान्।
मातृरक्षःपिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान्॥
अनुवाद:
भगवान ने किन्नरों, अप्सराओं, नागों, सर्पों, किम्पुरुषों और अन्य सभी जीवों का सृजन किया है। उन्होंने मातृ रक्षा, पिशाचों, प्रेतों और भूतों के विनाश का कार्य भी किया।
श्लोक 39:
कूष्माण्दोन्माद वेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि।
खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप सरीसृपान्॥
अनुवाद:
भगवान ने कूष्माण्डों, उन्मादित भूतों, वेतालों, यक्षों, ग्राहों और खगों (पक्षियों), मृगों, पशुओं, वृक्षों, पर्वतों, सरीसृपों (साँपों) का भी सृजन किया है।
श्लोक 40:
द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जल स्थल वनौकसः।
कुशला-अकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः॥
अनुवाद:
कुछ जीव जल, स्थल और आकाश में रहते हैं, और उनके कर्म कुशल, अकुशल या मिश्रित होते हैं। यह सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने मार्ग पर अग्रसर होते हैं।
श्लोक 41:
सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुर-नृ-नारकाः।
तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा।
यद् एकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते॥
अनुवाद:
सभी जीवों को तीन गुण—सत्त्व, रजस और तमस—के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है: देवता, मनुष्य, और नरकवासी। इन गुणों का प्रभाव समय के साथ इन जीवों की गति को विभाजित करता है।
श्लोक 42:
स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक्।
पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ्नरसुरादिभिः॥
अनुवाद:
भगवान ही इस संसार के रचनाकार हैं और धर्म के रूप में सभी का पालन करते हैं। वे तिर्यक् (जंगली जीवों), मनुष्यों और देवताओं से लेकर सभी जीवों के पालनकर्ता हैं।
श्लोक 43:
ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टं इदमात्मनः।
सं नियच्छति तत्काले घनानीकं इवानिलः॥
अनुवाद:
फिर काल (समय) और आग्नि (आग) की तरह भगवान सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। वह समय के अनुसार जीवन को चला कर घनकारी और आकाश के समान सब कुछ व्यवस्थित करते हैं।
श्लोक 44:
इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः।
न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुं अर्हन्ति सूरयः॥
अनुवाद:
भगवान ने अपने सर्वोत्तम रूप को इस प्रकार प्रकट किया है। कोई भी सूरज जैसे दिव्य दृष्टि वाले भी उनके परम रूप को इस भाव से देखने योग्य नहीं हैं।
श्लोक 45:
नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते।
कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्॥
अनुवाद:
भगवान के कर्मों में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। उनकी कार्यों को समझने के लिए माया का अंश होता है, ताकि सभी कर्मों का संचालन किया जा सके।
श्लोक 46:
अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः।
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः॥
अनुवाद:
यह ब्रह्मा के द्वारा रचित कल्प है, जिसमें सृष्टि के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृत और वैकृत सर्ग (सृष्टि) होते हैं।
श्लोक 47:
परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम्।
यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो श्रृणु॥
अनुवाद:
समय का विस्तार और कल्प के लक्षण को बताने के लिए मैं इस पाद्म कल्प का वर्णन करूंगा। सुनो, यह प्रक्रिया बहुत महान और रहस्यमय है।
शौनक उवाच
श्लोक 48:
यदाह नो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः।
चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बंधून् सु-दुस्त्यजान्॥
अनुवाद:
शौनक ने पूछा: "हे सूत! आप जो भागवत की उत्तम कथा कहते हैं, वह हमें सुनाने के लिए साक्षात्कार किया गया था। आपने तीर्थ यात्रा की और बंधुओं के दुखों को समाप्त किया।"
श्लोक 49:
क्षत्तुः कौशारवेः तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः।
यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्टः तत्त्वं उवाच ह॥
अनुवाद:
वह संवाद जिसे आपने बताया, वह कौशारव के साथ था और वह आध्यात्मिक शिक्षा से भरपूर था। आपने भगवान से पूछा और उन्होंने तत्त्व के बारे में बताया।
श्लोक 50:
ब्रूहि नः तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्।
बन्धुत्याग निमित्तं च यथैव आगतवान् पुनः॥
अनुवाद:
शौनक ने सूत से पूछा: "हमें यह बताएं कि विदुर ने किस कारण से बंधु-त्याग किया और क्यों वह पुनः लौटे?"
सूत उवाच
श्लोक 51:
राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद् अवोचत् महामुनिः।
तद्वोऽभिधास्ये श्रृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः॥
अनुवाद:
सूत जी ने उत्तर दिया, "राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा है, वह महात्मा विदुर के बारे में है। मैं उसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कृपया ध्यान से सुनें।"
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥
इस प्रकार श्रीमद्भागवतम् महापुराण में पारमहंस संहिता में द्वितीय स्कंध का दसवां अध्याय समाप्त हुआ।
इस प्रकार यहाँ पर भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय(हिन्दी अनुवाद) के सभी श्लोकों के साथ हिन्दी अनुवाद क्रमशः प्रस्तुत किया गया।